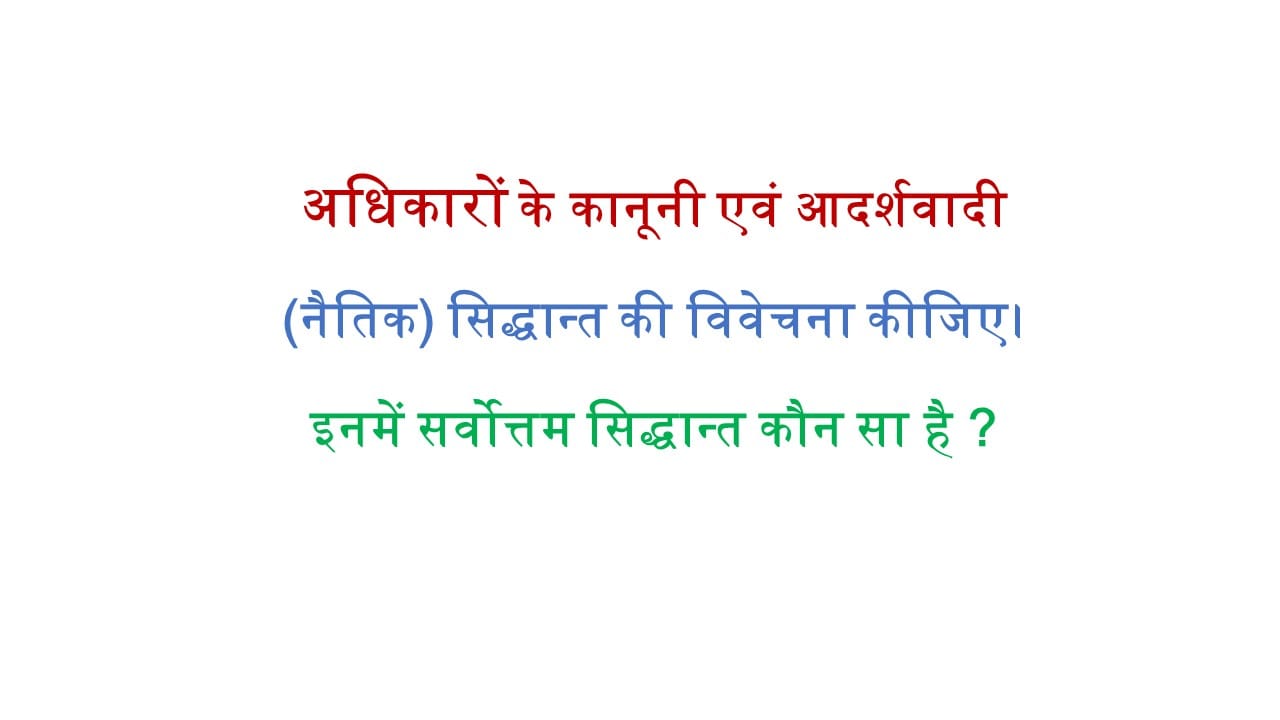प्रश्न- अधिकारों के कानूनी एवं आदर्शवादी (नैतिक) सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। इनमें सर्वोत्तम सिद्धान्त कौन सा है ?
अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त
(Legal Theory of Rights)
अधिकारों के कानूनी सिद्धान्त के अनुसार, अधिकार राज्य द्वारा निर्मित कानून की देन हैं। ये राज्य की इच्छा तथा कानून का परिणाम होते हैं। उन्हीं अधिकारों का हम वास्तविक रूप से उपभोग कर सकते हैं, जिन्हें कानून मान्यता देता है । जिन अधिकारों को कानून मान्यता नहीं देता है वे अधिकार नहीं होते हैं। अधिकार प्राकृतिक तथा निरपेक्ष नहीं होते हैं। वे देश, समय व परिस्थिति के अनुसार कानून की देन होते हैं। राज्य कानूनों के माध्यम से नए अधिकारों को जन्म देता है तथा पुराने अधिकारों को समाप्त भी कर सकता । इस प्रकार अधिकार कृत्रिम हैं, स्वाभाविक या प्राकृतिक नहीं । जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के अधिकार कानून की देन हैं। इन सबका निर्धारण राज्य करता है। प्राकृतिक अधिकारों का आधार भी कानून ही हैं क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार अनावश्यक है तथा कानून से मेल नहीं खाते, उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है।
बेन्थम, ऑस्टिन व हॉलैण्ड आदि विचारकों ने इस कानूनी अधिकार के सिद्धान्त का समर्थन किया है। बेन्थम के अनुसार, “उचित अर्थ में अधिकार विधि की ही कृति हैं।’ आधुनिक काल में इसे यथार्थवादी सिद्धान्त कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार अधिकार का आधार नैतिकता नहीं वरन् यथार्थ है तथा उसका आधार राज्य और कानून है।
आलोचना : अधिकारों के कानूनी सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार से की गई है-
1. राज्य अधिकारों का एकमात्र स्त्रोत नहीं है : राज्य या कानून के आदेश मात्र से कोई अधिकार नहीं बन जाता है। नार्मन वाइल्ड (Norman Wilde ) के अनुसार, “राज्य हमारे अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता, वह केवल उन्हें मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। अधिकार का अस्तित्व स्वयं अपने आप में रहता है। उन्हें कानून का रूप चाहे मिले या न मिले, कानून द्वारा उन्हें इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि वे अधिकार हैं। कानून द्वारा क्रियान्वित किए जाने के कारण वे अधिकार नहीं बनते।”
2. कानून अधिकारों का उचित आधार नहीं हैं : अधिकारों के कानूनी सिद्धान्त को मानने से राज्य स्वेच्छाचारी और निरंकुश बन जाएगा। डॉ० आशीर्वादम के अनुसार, “”यह कहना कि एकमात्र राज्य ही अधिकारों की सृष्टि करता है, राज्य को निरंकुश बना देना है।” राज्य के कार्यों की कुछ सीमाएँ होती हैं जैसे कि नैतिकता, रीति-रिवाज, परम्परा, इतिहास तथा जनमत आदि ।
3. समाज को मान्यता नहीं देता है : यह सिद्धान्त अधिकारों पर समाज की स्वीकृति को मान्यता नहीं देता है। वास्तव में अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही कानूनी रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार राज्य कानूनी अधिकारों का एकमात्र निर्माता नहीं है।
4. राज्य के निरंकुश होने का भय : इससे राज्य को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप राज्य के स्वेच्छाचारी व निरंकुश हो जाने की सम्भावना बढ़ जाती है। यद्यपि इस सिद्धान्त की अनेक प्रकार से आलोचनाएँ की गई हैं तथापि इस सिद्धान्त में सत्य का अंश है। वस्तुतः राज्य की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अधिकारों के नैतिक तथा कानूनी दो पक्ष होते हैं। अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए कानूनी मान्यता आवश्यक है। बोदाँ के शब्दों में, “अधिकारों के कानूनी तथा नैतिक दोनों पक्ष होते हैं।”
नैतिक सिद्धान्त
(Moral Theory)
इस सिद्धान्त की मान्यता के अनुसार अधिकार वे बाह्य परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति के आन्तरिक नैतिक विकास के लिए अनिवार्य होती हैं। परिस्थितियाँ अथवा दशाएँ व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास इन्हीं पर निर्भर करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए इन दशाओं का होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए ये अधिकार हैं। वाइल्ड के अनुसार “कुछ कार्यों का सम्पादन करने की आवश्यकता स्वतन्त्रता के लिए उन तर्कपूर्ण दावों का नाम अधिकार है जो व्यक्ति की उन्नति के लिए परमावश्यक होते हैं।” वस्तुतः अधिकार मानव विकास की आवश्यक शर्तों का ही दूसरा नाम है। मनुष्य कुछ कार्यों को करने के लिए कुछ दावे या माँगें रखता है। ये दावें या माँगें यदि उसके अस्तित्व तथा नैतिक विकास के लिए अनिवार्य हैं तो अधिकार कहलाते हैं। ग्रीन के अनुसार, “अधिकार वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीवन के रूप में उसके व्यवसाय और कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है।”
यह सिद्धान्त अधिकारों को प्राकृतिक नहीं मानता है वरन् यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ शक्तियों के साथ इस विश्व में उत्पन्न होता है। इन शक्तियों के विकास के लिए जीवित रहना, शिक्षा व भोजन आवश्यक है तो जीवन, शिक्षा व भोजन उसके अधिकार हैं। इस प्रकार यह सिद्धान्त अधिकारों को व्यक्तित्व की शक्तियों के विकास से सम्बन्धित कर देता है। आदर्शवादी सिद्धान्त के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं-
(1) अधिकारों का अस्तित्व समाज में है।
(2) अधिकार मानव स्वभाव में निहित हैं। (3) प्रत्येक अधिकार में कर्त्तव्य भी निहित है ।
(4) व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं वरन प्राकृतिक शक्तियाँ लेकर उत्पन्न होता है।
(5) व्यक्ति के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करने का कार्य समाज एवं राज्य के द्वारा किया जाता है।
( 6 ) व्यक्ति स्वयं में साध्य है, अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है।
(7) व्यक्ति को केवल वे ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं।
(8) एक व्यक्ति के अधिकारों पर उतने ही प्रतिबन्ध लगाए जाएँ जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित न करें।
आलोचना : आदर्शवादी सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है—
1. सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं : यह सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है क्योंकि व्यक्तित्व का विकास व्यक्तिगत पहलू है तथा समाज व राज्य जैसी संस्था के लिए यह जानना बहुत कठिन है कि किसके विकास के लिए क्या आवश्यक है।
2. समाज को गौण स्थान देता है : यह व्यक्ति के हितों पर अधिक बल देता है और समाज का स्थान गौण रखता है, अतः व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समाज के हितों के विरुद्ध कार्य कर सकता है।
3. आधारशिला अवैज्ञानिक : मानव जीवन के विकास की आवश्यक परिस्थितियाँ कौन-सी हैं, इनका निर्णय कौन करेगा तथा ये कैसे उपलब्ध होंगी- इस सिद्धान्त में इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं होता है। अतः इस सिद्धान्त की आधारशिला अवैज्ञानिक है।
यह सिद्धान्त इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को वे ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं। यह इस बात पर भी बल देता हैं कि व्यक्ति स्वयं साध्य है, साधन मात्र नहीं हैं। यह सिद्धान्त अधिकार के नैतिक पक्ष पर बल देता है।
सर्वोत्तम सिद्धान्त
(Most Appropriate Theory)
तर्क की दृष्टि से अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धान्त सर्वोत्तम है। अन्य सिद्धान्त अधिकारों को निरपेक्ष, प्रकृति प्रदत्त अथवा राज्य के प्रभुत्व में निहित मानते हैं, जो अधिकारों की प्रकृति एवं महत्त्व पर समुचित प्रकाश नहीं डालते हैं। यही एकमात्र सिद्धान्त है जो अधिकारों को व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध करके उसके औचित्य को सिद्ध करने में सफल रहा है। इस सिद्धान्त में कुछ दोष भी निहित हैं, परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता यह राज्य तथा व्यक्ति के सम्बन्धों की उचित व्याख्या करता है। अतः यह विवाद समाप्त हो जाता है कि अधिकार कौन-कौन से होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य होता है तथा अन्य के लिए साधन नहीं बनता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के रूप में हमें ऐसा मापदण्ड मिल जाता है जिससे अधिकारों की जाँच की जा सके। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कि व्यक्तित्व के विकासरूपी आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह व्यक्ति का अधिकार है, उचित प्रतीत होता है।